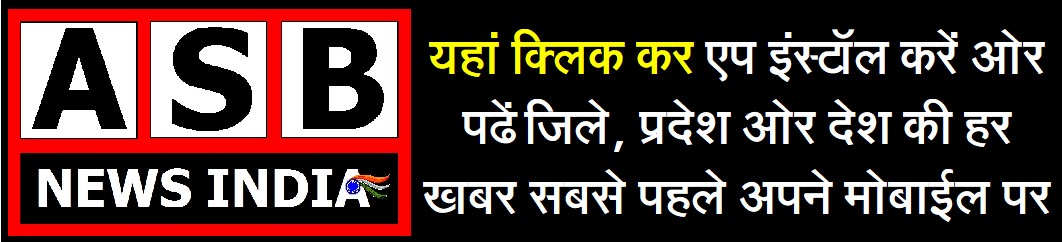
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कानून निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करेगी। हालांकि पिछले एक साल से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ़ कर दिया है कि तीनों कानून की वापसी और एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी मिलने के बाद ही किसान अपना प्रदर्शन वापस लेंगे। मोदी सरकार पर फसलों के एमएसपी को क़ानूनी गारंटी प्रदान किए जाने का दवाब बढ़ रहा है। आइये जानते हैं कि आखिर एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग क्यों की जा रही है और इसको पूरा करने से सरकार को क्या नुकसान है? साथ ही इसके वित्तीय और दूसरे क्या प्रभाव हो सकते हैं?
केंद्र वर्तमान में 23 फसलों को एमएसपी देता है। इनमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर), 7 तिलहन (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल) शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 4 व्यावसायिक फसलें (गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट) भी शामिल है। एमएसपी तकनीकी रूप से खेती में लगने वाले कुल लागतों के न्यूनतम 50% वापसी को सुनिश्चित करता है। हालांकि यह काफी हद तक कागज़ पर ही है। भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलों में से किसानों को विशेष रूप से फसल के समय प्राप्त होने वाली कीमतें आधिकारिक तौर पर घोषित एमएसपी से काफी कम होती हैं। चूंकि एमएसपी को लेकर कोई वैधानिक गारंटी नहीं है इसलिए किसान इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हैं। इसलिए किसान संगठन चाहते हैं कि मोदी सरकार केवल सांकेतिक मूल्य के बजाय एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून बनाए।
इसके मूल रूप से तीन तरीके हैं। पहला प्राइवेट व्यापारियों को अनिवार्य रूप से एमएसपी का भुगतान करने के लिए कहना। हालांकि गन्ने को लेकर यह पहले से ही लागू है। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मूल्य के अनुसार चीनी मिलों को गन्ना किसानों को उचित और लाभाकारी मूल्य देना पड़ता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर कानूनी रूप से गारंटी मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। 2020-21 चीनी वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के आंकड़ों के अनुसार चीनी मिलों ने लगभग 298 मिलियन टन गन्ने की पेराई की जो देश के 399 मिलियन टन के कुल अनुमानित उत्पादन के तीन-चौथाई के करीब था।
दूसरा है भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय कपास निगम (CCI) जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से MSP पर सरकारी खरीद। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में हुए चावल के उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा एमएसपी पर ख़रीदा गया, जबकि गेहूं के लिए यह आंकड़ा 40% और कपास में 25% से अधिक था।
सामान्यतया एमएसपी केवल चार फसलों गन्ना, धान, गेहूं और कपास में प्रभावी रहा है। हालांकि आंशिक रूप से पांच फसलों चना, सरसों, मूंगफली, अरहर और मूंग में और शेष 14 अधिसूचित फसलों में काफी कमजोर रहा है। पशुधन और बागवानी उत्पादों चाहे दूध, अंडे, प्याज, आलू या सेब हो इसपर सरकार की तरफ से कोई एमएसपी नहीं दिया जाता है। वानिकी और मछली पकड़ने को छोड़कर जिन 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है वो भारत के कृषि उत्पादन में मुश्किल से एक तिहाई का योगदान देता है।
एमएसपी की गारंटी के लिए तीसरा माध्यम मूल्य न्यूनता भुगतान है। इसके तहत सरकार न तो सीधे खरीद करती है और न ही निजी घरानों को एमएसपी देने के लिए मजबूर करती है। इसके बजाय यह किसानों को सभी बिक्री को मौजूदा बाजार कीमतों पर करने की अनुमति देता है। किसानों को केवल सरकार के द्वारा तय किए गए एमएसपी और कटाई के मौसम के दौरान फसल के लिए औसत बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है।
साल 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार एमएसपी मिलने वाले सभी 23 फसलों के कुल उत्पादन का एमएसपी मूल्य लगभग 11.9 लाख करोड़ है। लेकिन सभी उपज एमएसपी पर नहीं बेचीं जाती है। किसानों के द्वारा खुद रखे जाने, बीज और पशुओं के लिए खिलाने के बाद ही बचे फसलों को एमएसपी पर बेचा जाता है। अगर सभी फसलों का औसत 75 % उत्पादन ही लिया जाए तो किसानों द्वारा वास्तव में बेचे गए उत्पादन का एमएसपी मूल्य 9 लाख करोड़ से भी कम है।
2020-21 के दौरान खरीदे गए 89.42 मिलियन धान और 43.34 मिलियन टन गेहूं का एमएसपी मूल्य लगभग 253,275 करोड़ रुपये था। इसके अलावा नेफेड द्वारा खरीदे गए दलहन और तिलहन का एमएसपी मूल्य 2019-20 में 21,901 करोड़ रुपये और 2020-21 में 4,948 करोड़ रुपये है। साथ ही कपास निगम द्वारा ख़रीदे गए कपास या कच्चे कॉटन का एमएसपी 2019 में 28,420 करोड़ रुपये और 2020-21 में 26,245 करोड़ रुपये है। इसके अलावा गन्ना मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने का एमएसपी मूल्य 2020-21 में 92,000 करोड़ रुपये भी है।
















