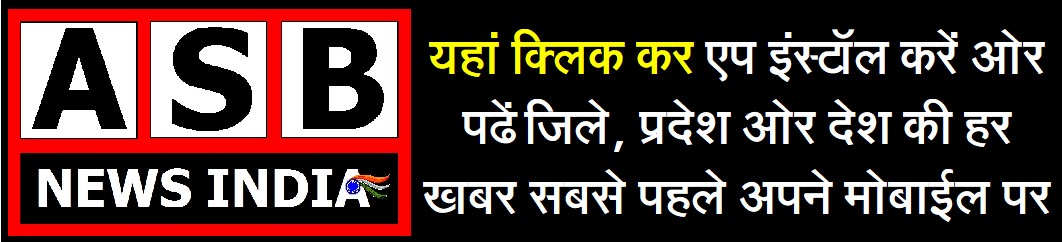
नई दिल्ली. 19 नवंबर 2021 भारत के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल से चल रहे आज़ाद भारत के अब तक के सबसे बड़े आंदोलन का पटाक्षेप करते हुए, तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन, सबसे पहले केंद्र सरकार कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पर ही काम करेगी. इस कानून के विरोध में एक साल से दिल्ली की सीमा पर बैठे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अभी यहां से उठने के मूड में नहीं हैं. भले ही केंद्र सरकार को लग रहा था कि उसने आंदोलन का अंतिम दृश्य लिख दिया है, लेकिन तभी किसानों ने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी के लिए भी कानून बनाने पर अड़ गए हैं. इस मांग को पूरा करने पर क्या होगा वित्तीय प्रभाव…
आखिर क्यों यूनियन कर रही है एमएसपी की मांग?
केंद्र ने हाल ही में 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की थी, जिसमें 7 अनाज ( धान, गेंहू, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और 5 दलहन (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर) 7 तिलहन (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लॉवर, कुसुम, तिलस नाइजरसीड) और 4 व्यवसायिक फसल (गन्ना, कपास, कोपरा और कच्चा जूट) शामिल हैं. कागजों पर एमएसपी तकनीकी तौर पर सभी फसलों के कम से कम 50 फीसद लागत की वापसी सुनिश्चित करती है.
भारत के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए किसानों को जो दाम मिलते हैं, वह आमतौर पर घोषित एमएसपी से काफी कम होते हैं. चूंकि एमएसपी को लेकर कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है इसलिए किसान इसे अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकते हैं. अब यूनियनों की मांग है कि मोदी सरकार वांछित या सांकेतिक मूल्य के बजाए एमएसपी को लेकर अनिवार्य दर्जा देने वाला कानून बनाए.
इसे लागू करने के तीन तरीके हो सकते हैं-
पहला तरीका तो यह है कि निजी व्यापारियों और प्रोसेसर पर एमएसपी के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाए. गन्ने की फसल पर यह कानून पहले से ही लागू है. चीनी मिलों को कानून के तहत किसानों को केंद्र द्वारा तय किए गये उचित और लाभकारी दाम चुकाना होता है. कुछ मामलों में राज्य सरकारें सुझाए गए दाम से भी अधिक दाम तय करती हैं. आवश्यक वस्तु अधिनियम (1996) के तहत कानूनी रूप से गन्ना खरीद के 14 दिनों के अंदर भुगतान करना ज़रूरी होता है.
दूसरा तरीका है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) जैसी एजेंसियों के जरिए एमएसपी पर सरकारी खरीद की जाए. इस तरह की खरीद में पिछले साल भारत के धान का उत्पादन का लगभग 50 फीसद, गेंहू का 40 फीसद और कपास का 25 फीसद से अधिक हिस्सा था. सरकारी एजेंसियों ने 2019-20 के दौरान चना, सरसों, मूंगफली, अरहर और मूंग की उल्लेखनीय खरीदी की थी. इनमें से अधिकतर अप्रैल-जून 2020 के दौरान खरीदी गई जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. हालांकि 2020-21 में इन फसलों की खरीद में गिरावट दर्ज हुई. सरसों, अरहर, मूंग, मसूर और सोयाबीन के मामले में खरीद की जरूरत महसूस ही नहीं की गई थी क्योंकि खुले बाजार के दाम एमएसपी से ज्यादा थे.
सामान्यतौर पर एमएसपी 4 फसलों पर ही प्रभावी रहा है (गन्ना, धान, गेंहू, और कपास), आंशिक तौर पर 5 (चना, सरसों, मूंगफली, अरहर और मूंग) और बाकी 14 कमजोर अधिसूचित फसल हैं. वहीं पशुधन, उद्यानिकी के उत्पाद, दूध, अंडा, प्याज, आलू और सेब पर कागजों में कोई एमएसपी दर्ज नहीं है. जो 23 फसलें एमएसपी में शामिल हैं वो भारत की कुल फसल का एक तिहाई भी नहीं हैं.
तीसरा तरीका दाम की कमी के भुगतान के जरिए निकलता है. इसके तहत सरकार ना तो सीधी खरीद करती है और ना ही निजी उद्योग को एमएसपी देने के लिए मजबूर करती है. बल्कि वह किसानों को मौजूदा बाजार की कीमत पर बिक्री की अनुमति देती है. इसमें सरकार को किसानों को फसल की कटाई के दौरान सरकार की एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के बीच का भुगतान करना होता है.
एमएसपी पर कानून बनने की क्या कीमत होगी?
सभी 23 अधिसूचित फसलों की 2020-21 में कुल एमएसपी लागत 11.9 लाख करोड़ थी, लेकिन इन सारे उत्पाद का विपणन नहीं हुआ था. विपणन की अधिकता अनुपात, किसानों के खुद के इस्तेमाल, बीज, पशुओं को खिलाने के बाद जो बचता है उससे निकाला जाता है. किसानों द्वारा जो वास्तव में बेचे गए उत्पादन का एमएसपी मूल्य 9 लाख करोड़ रुपये के अंदर था. सरकार आगे भी कई फसल खरीद रही है. जिसमें 89.42 मीट्रिक टन धान और 43.44 मीट्रिक टन गेंहू जो 2020-21 में खरीदा गया था उसकी एमएसपी लागत 253 और 275 करोड़ थी. इसमें नेफेड ने जो दलहन और तिलहन की खरीद की उसकी 2019-20 में 21,901 करोड़ और 2020-21 में इसकी एमएसपी लागत 4,948 करोड़ रु थी. और सीसीआई ने जो कपास (2019-20 में 28420 करोड़ रु) खरीदा उसे भी शामिल करना होगा.
















